सिस्टम के सिंडिकेट का खेल जारी, पुष्पेंद्र बागरी पर कार्रवाई से परहेज क्यों?….
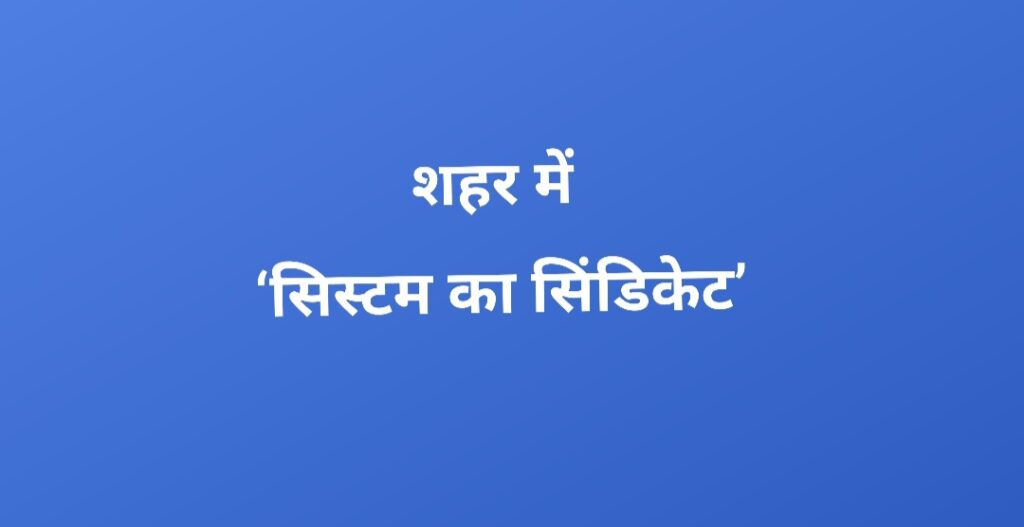
सतना। जिले भर में प्रधान आरक्षक पुष्पेंद्र बागरी का ‘सिस्टम का सिंडिकेट’ बेधड़क जारी है। पशु तस्करी, सट्टा, अवैध शराब और जुए के अवैध कारोबार को संरक्षण देने की चर्चाएं बनी हुई हैं। सूत्रों का दावा है कि तीनों थानों में उनके अपने मुखबिर तैनात हैं, जो हर सूचना उन्हें पहुंचाते हैं। एयरपोर्ट में ड्यूटी होने के बावजूद रात में बाईपास और शहर की संदिग्ध गलियों में उनकी गाड़ी देखी जाती है। हिस्सेदारी न देने पर कारोबारी की गाड़ियों की चेकिंग और फिर सौदेबाजी की बातें भी व्यापारियों की जुबान पर हैं।
थाना सूत्र बताते हैं कि पूर्व में लाइन हाजिर होने के बावजूद इनके नेटवर्क पर असर नहीं पड़ा। हैरानी की बात है कि सब कुछ जानते हुए भी वरिष्ठ अफसर कार्रवाई से परहेज कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर पुष्पेंद्र पर प्रशासन मेहरबान क्यों है? क्या उनके राजनीतिक संपर्क या सिस्टम में मजबूत पकड़ अधिकारियों की मजबूरी बन गई है, या फिर शहर की शांति की कीमत उनके सिंडिकेट से तय की जा चुकी है? फिलहाल, सतना में पुष्पेंद्र जैसे शिपाहियो की छत्रछाया में अवैध कारोबार का यह खेल खुलेआम जारी है, ऐसी जन चर्चा है!
जानकार बताते हैं कि..👇
1️⃣ राजनीतिक संरक्षण: पुष्पेंद्र के पीछे कुछ स्थानीय नेताओं और ठेकेदारों का संरक्षण बताया जाता है, जिससे अधिकारी कार्रवाई से कतराते हैं।
2️⃣ सूचना तंत्र में पकड़: थानों और सीएसपी ऑफिस तक उनकी पकड़ होने से अधिकारियों की हर गतिविधि की जानकारी उनके पास पहले पहुंच जाती है।
3️⃣ लेनदेन की व्यवस्था: सिंडिकेट से होने वाली कमाई का हिस्सा ऊपर तक पहुंचने की चर्चा है, जिससे कार्रवाई की फाइलें बंद पड़ी रहती हैं। हालांकि पुलिस अधीक्षक तक इनके लेनदेन व अवैध गतिविधियों की जानकारियां नहीं होने दी जाती है।
4️⃣ स्थानीय नेटवर्क: थाना सूत्र बताते हैं की बागरी ने थानों में अपने लोगों को तैनात कर रखा है, जिससे पुलिसिया कार्रवाई पर भी नियंत्रण बना रहता है।
5️⃣ खौफ और सौदेबाजी: कारोबारी उनके खौफ और सौदेबाजी से दबे रहते हैं, जिससे खुली शिकायतें सामने नहीं आतीं।
6️⃣ प्रशासनिक चुप्पी की कीमत: कई व्यापारी मानते हैं कि उच्च स्तर पर भी ‘सौदा’ तय होने के कारण प्रशासन मौन साधे बैठा है।
